निगाहें ढूंढती है गाँव के उन बाजारों को...
निगाहें ढूंढती है गाँव के उन बाजारों को...
गाँवो में बाजार लगाने की सालो पुरानी प्रथा अब विलुप्ति के कगार पर है। एक समय था जब प्रत्येक गाँव में निर्धारित दिन/तिथि को बाजार लगता था। कुछ समय पहले तक शहरों की तरह गावों में स्थाई दुकाने नही हुआ करती थी। कई घरो के चूल्हे इन बाजारों से होनी वाली आमदनी से जला करते थे। तब कम पूंजी वाले दुकानदार भी आसानी से अपनी चलती-फिरती दुकान लगाया करते थे। उन्हें इन दुकानो को लगानें के एवज में जमीन मालिक को या तो मामूली रकम अदा करनी होती थी या फिर उसके बदले में समान दे दिया करते थे। कई दफा तो दरियादिली में लोग उन्हें मुफ़्त में ही दुकान लगाने दिया करते थे।
अब बाजार के उन छोटे दुकानों की जगह स्थाई दुकाने लगती है। हजारों की रकम उसके एवज में जमा की जाती है। नतीजतन स्वतः ही समानो के दाम बढ़ जाते है। हाँ ये सच है कि अब जब जरूरत होती है,हमे पसंद या जरूरत की वस्तुएं उसी वक्त मिल जाती है। परन्तु इस बाजारवाद के नए स्वरूप ने सैकड़ो छोटे दुकानदारो को उनके पारम्परिक पेशे से जुदा भी तो किया है।
तब लोग मिल-बाटकर अपनी जरूरते पूरी कर लेते थे। लोग समूहों में बाजार जाते थे,अत: गाँव-जवार के लोगों के मिलन का एक केंद्र होते थे ये बाजार। अब जिसे जिस की जरूरत है वह उसी वक्त खरीद लाता है। पहले लोग एक दूसर से मांगकर अपनी जरूरते पूरी किया करते थे जिससे आपसी प्रेम और सोहार्द बना रहता था। अब वो भाईचारा भी खात्मे की ओर है....
अपने विचार दे।
अनुराग रंजन
छपरा(मशरख)

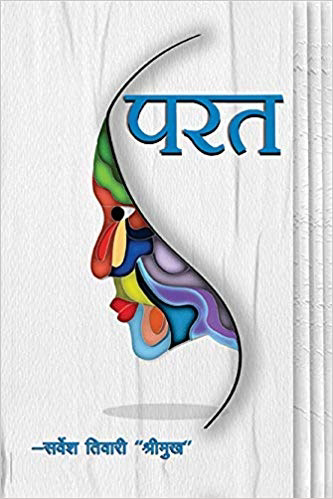

Comments
Post a Comment